अनंत की ओर.........
जब - जब नाना जी का ज़िक्र आता है, तब - तब मन पीछे की ओर चल पडता है। और चलते- चलते उसी 19 अप्रैल, 1998 की उसी धुन्धली तारीख पर पहुँच जाता है, जब नाना जी हम सब से दूर, एक अंतहीन सफ़र पर चले गए थे।
ज़ेहन पर जमी धूल को थोड़ा और साफ करुँ तो आँखों के आगे एक तस्वीर उभरती है, जिसमें अप्रैल की एक गनगुनी गर्मी वाली एक सुबह, मैं खुद को एक काली बुलेट मोटरसाइकिल की टंकी पर बैठा हुआ पाता हूँ। हाथ में बुलेट की चाभी है जिसको लेकर मैं उसकी टंकी पर कुछ उकेरने की जद्दोजहद कर रहा हूँ, जैसा की 2 साल के बच्चे अमूमन करते हैं।
मेरे बाएँ हाथ की ओर एक शख्स भी है जो अपने हाथों से मुझे थामे हुए है ताकी मैं गिर ना पडूँ। कुछ देर बाद वहीं बगल में खड़ा शख्स अचानक मुझे गोद में उठा लेता है और कहने लगता है - 'बाबू नाना जी को चाभी दे दो।'
इससे पहले मैं कुछ समझ पता चाभी मेरे हाथों से ली जा चुकी थी। नाना जी ने मेरे तरफ देखते हुए बाय का इशारा किया। वह सज्जन जो मुझे गोद में लिए हुए थे, उनकी आवाज़ कान में पड़ी- 'नाना जी को बाय कर दो'। इससे पहले की मैं उन्हें बाय कर पाता, नाना जी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कुछ दूर जा चुके थे। उसके बाद मैं कैसे अन्दर घर में गया और कब मैं नींद की आगोश में फिसल गया, इसका कोई ठीक - ठीक खाका मेरे ज़ेहन में नहीं है।
हाँ, नींद टूटने के बाद का मातम मंज़र बखूबी याद है। उस दिन के बाद से घर ना जाने कितनी ही बार रंगाई- पुताई हुई होगी, पर 19 अप्रैल के उस मातम का परछाई, घर की उन दीवारों पर आज भी जस की तस है।
होश संभाला तो पता लगा की उस दिन एक जाहिल आदमी की बेतरतीब ड्राईविंग का खामियाज़ा हमारे परिवार को उठाना पड़ा। कुछ और बडे हुए तो पता लगा की मैं उस शख्सियत का नाती हूँ जिसने उत्तर प्रदेश के एक सुदूर कोने पर बसे अहिरौली मिश्र नाम के देहात को, बिना किसी राजनीतिक पद पर रहे अपने निजी संसाधनों के बल पर बिजली, टेलीफोन, गौशला और डिग्री कॉलेज जैसी सौगातें दीं।
नाना जी की शख्सियत की विराट काया का अन्दाजा मुझे वास्तव में आज हुआ, जब मेरे ननिहाल के पास के गाँव का एक अधेड़ उम्र के फल विक्रेता ने यह पता लगने पर मुझ से पैसे लेने से इंकार कर दिया, की मैं 'चौबे जी का नाती हूँ'। बकौल फल विक्रेता अरसे पहले उसके बच्चे के इलाज में मेरे नाना जी ने कोई अर्थिक सहायता दी थी। बस इसी संयोग ने इस पोस्ट को लिखने पर मजबूर कर दिया।
अभी पार्क की बेंच पर बैठे- बैठे जब उंगलियाँ बिजली की तेज़ी से फ़ोन की स्क्रीन पर नाच रही हैं, तो दिल का एक हिस्सा, दिमाग से रह-रहकर पूछ रहा है क्या उस दिन मैं थोड़ी सी ज़िद और नहीं कर सकता था? संभव है की अगर मैं थोड़ी सी ज़िद और करके, चाभी को अपने हाथों में भींच लेता, तो शायद नाना जी उस दिन जाते ही नहीं! ख्याल तो कभी - कभी यह भी आता है की मैं शायद कभी 19 अप्रैल की उस नींद से जागा ही नहीं?
और संभवतः जिसे मैं आज अपना वर्तमान मानकर जी रहा हूँ, वह वर्तमान नहीं बल्कि 19 अप्रैल की उसी नींद का ही एक सपना है।
सपना जो किसी भी पल टूटेगा, जब नाना जी मुझे आकर जगाएंगे और गोद में उठाकर बारांडे की ओर चल देंगे.........
ज़ेहन पर जमी धूल को थोड़ा और साफ करुँ तो आँखों के आगे एक तस्वीर उभरती है, जिसमें अप्रैल की एक गनगुनी गर्मी वाली एक सुबह, मैं खुद को एक काली बुलेट मोटरसाइकिल की टंकी पर बैठा हुआ पाता हूँ। हाथ में बुलेट की चाभी है जिसको लेकर मैं उसकी टंकी पर कुछ उकेरने की जद्दोजहद कर रहा हूँ, जैसा की 2 साल के बच्चे अमूमन करते हैं।
मेरे बाएँ हाथ की ओर एक शख्स भी है जो अपने हाथों से मुझे थामे हुए है ताकी मैं गिर ना पडूँ। कुछ देर बाद वहीं बगल में खड़ा शख्स अचानक मुझे गोद में उठा लेता है और कहने लगता है - 'बाबू नाना जी को चाभी दे दो।'
इससे पहले मैं कुछ समझ पता चाभी मेरे हाथों से ली जा चुकी थी। नाना जी ने मेरे तरफ देखते हुए बाय का इशारा किया। वह सज्जन जो मुझे गोद में लिए हुए थे, उनकी आवाज़ कान में पड़ी- 'नाना जी को बाय कर दो'। इससे पहले की मैं उन्हें बाय कर पाता, नाना जी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कुछ दूर जा चुके थे। उसके बाद मैं कैसे अन्दर घर में गया और कब मैं नींद की आगोश में फिसल गया, इसका कोई ठीक - ठीक खाका मेरे ज़ेहन में नहीं है।
हाँ, नींद टूटने के बाद का मातम मंज़र बखूबी याद है। उस दिन के बाद से घर ना जाने कितनी ही बार रंगाई- पुताई हुई होगी, पर 19 अप्रैल के उस मातम का परछाई, घर की उन दीवारों पर आज भी जस की तस है।
होश संभाला तो पता लगा की उस दिन एक जाहिल आदमी की बेतरतीब ड्राईविंग का खामियाज़ा हमारे परिवार को उठाना पड़ा। कुछ और बडे हुए तो पता लगा की मैं उस शख्सियत का नाती हूँ जिसने उत्तर प्रदेश के एक सुदूर कोने पर बसे अहिरौली मिश्र नाम के देहात को, बिना किसी राजनीतिक पद पर रहे अपने निजी संसाधनों के बल पर बिजली, टेलीफोन, गौशला और डिग्री कॉलेज जैसी सौगातें दीं।
नाना जी की शख्सियत की विराट काया का अन्दाजा मुझे वास्तव में आज हुआ, जब मेरे ननिहाल के पास के गाँव का एक अधेड़ उम्र के फल विक्रेता ने यह पता लगने पर मुझ से पैसे लेने से इंकार कर दिया, की मैं 'चौबे जी का नाती हूँ'। बकौल फल विक्रेता अरसे पहले उसके बच्चे के इलाज में मेरे नाना जी ने कोई अर्थिक सहायता दी थी। बस इसी संयोग ने इस पोस्ट को लिखने पर मजबूर कर दिया।
अभी पार्क की बेंच पर बैठे- बैठे जब उंगलियाँ बिजली की तेज़ी से फ़ोन की स्क्रीन पर नाच रही हैं, तो दिल का एक हिस्सा, दिमाग से रह-रहकर पूछ रहा है क्या उस दिन मैं थोड़ी सी ज़िद और नहीं कर सकता था? संभव है की अगर मैं थोड़ी सी ज़िद और करके, चाभी को अपने हाथों में भींच लेता, तो शायद नाना जी उस दिन जाते ही नहीं! ख्याल तो कभी - कभी यह भी आता है की मैं शायद कभी 19 अप्रैल की उस नींद से जागा ही नहीं?
और संभवतः जिसे मैं आज अपना वर्तमान मानकर जी रहा हूँ, वह वर्तमान नहीं बल्कि 19 अप्रैल की उसी नींद का ही एक सपना है।
सपना जो किसी भी पल टूटेगा, जब नाना जी मुझे आकर जगाएंगे और गोद में उठाकर बारांडे की ओर चल देंगे.........



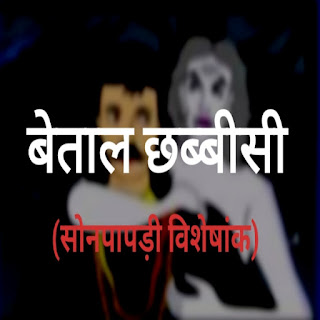

Comments
Post a Comment